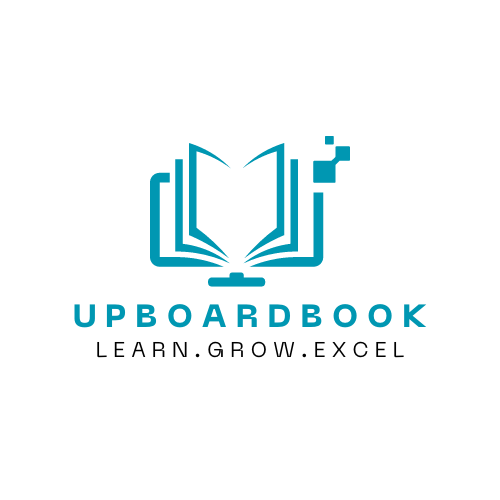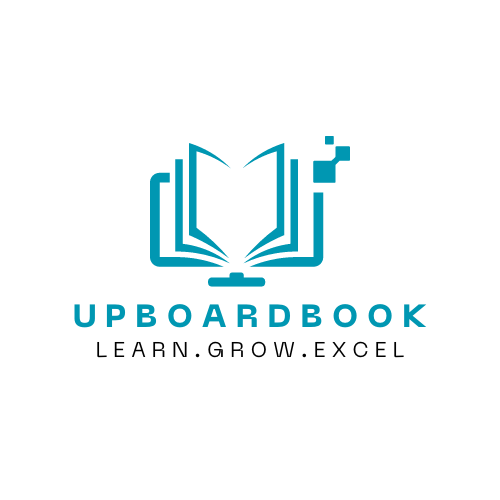UP Board class 12 Political Science Chapter 7. समकालीन विश्व सुरक्षा Hindi Medium Notes - PDF
अध्याय 7: समकालीन विश्व सुरक्षा
यह अध्याय सुरक्षा की अवधारणा और समकालीन विश्व में उसके बदलते स्वरूप पर केंद्रित है।
सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा
- केंद्रीय विचार: सुरक्षा का मतलब मुख्य रूप से सैन्य खतरों से सुरक्षा था।
- मुख्य उद्देश्य: देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना।
- मुख्य तरीका: सैन्य शक्ति का संचय और संधियाँ करना।
- शीत युद्ध का प्रभाव: इस दौरान सुरक्षा की यही अवधारणा प्रमुख थी, जिसमें दो महाशक्तियाँ (अमेरिका और USSR) शामिल थीं।
- सुरक्षा की इस सोच को 'राज्य-केंद्रित' सुरक्षा की संज्ञा दी जाती है।
सुरक्षा की व्यापक अवधारणा
- शीत युद्ध के बाद सुरक्षा के पारंपरिक दृष्टिकोण में बदलाव आया।
- सुरक्षा को सिर्फ सैन्य खतरों तक सीमित नहीं माना गया बल्कि इसमें गैर-सैन्य खतरों को भी शामिल किया गया।
- मुख्य विशेषताएँ:
- मानव-केंद्रित दृष्टिकोण: सुरक्षा का फोकस राज्य से हटकर व्यक्ति पर केंद्रित हो गया।
- सुरक्षा के अन्य आयाम: आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, सामुदायिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा जैसे नए आयाम जुड़े।
- इस नए दृष्टिकोण के तहत, गरीबी, बीमारी, अकाल, प्राकृतिक आपदाएँ, मानवाधिकार हनन आदि को भी सुरक्षा के लिए खतरा माना जाने लगा।
सुरक्षा के नए खतरे (नए स्रोत)
- आतंकवाद: यह एक प्रमुख वैश्विक खतरा बन गया है। इसका लक्ष्य आम नागरिक होते हैं और यह हिंसा के माध्यम से भय फैलाना चाहता है। उदाहरण: 9/11 की घटना।
- मानवाधिकार हनन: नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।
- ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय समस्याएँ: जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, संसाधनों की कमी आदि दीर्घकालिक सुरक्षा चुनौतियाँ हैं।
- साइबर खतरे: डिजिटल युग में साइबर हमले, डेटा चोरी, और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचाना नए प्रकार के खतरे हैं।
- सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) का प्रसार: परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों का गैर-राज्य कारकों के हाथों में पड़ने का खतरा।
- मानव तस्करी और नशीले पदार्थों की तस्करी: ये अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
विश्व सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीके
- सैन्य गठबंधन: NATO (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन) जैसे संगठन सामूहिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- निरस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और विश्वास-बहाली के उपाय:
- निरस्त्रीकरण: हथियारों को खत्म करने पर जोर, जैसे रासायनिक हथियार संधि (CWC)।
- शस्त्र नियंत्रण: हथियारों के प्रसार को सीमित करने की प्रक्रिया, जैसे परमाणु अप्रसार संधि (NPT)।
- विश्वास-बहाली के उपाय: देशों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने के लिए सूचना का आदान-प्रदान, संयुक्त सैन्य अभ्यास आदि।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका: संयुक्त राष्ट्र (UN) शांति स्थापना, संघर्ष रोकथाम और मानवीय सहायता के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देता है।
- सहयोग और वार्ता: द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता के माध्यम से तनावों को कम करना और सहयोग बढ़ाना।
भारत की सुरक्षा नीति
- भारत ने सुरक्षा के परंपरागत और व्यापक दोनों दृष्टिकोणों को अपनाया है।
- परंपरागत पहलू:
- मजबूत रक्षा बल और परमाणु शक्ति बनना।
- पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों का सामना करना।
- शांति और अहिंसा में विश्वास, लेकिन आत्मरक्षा में सक्षम।
- व्यापक पहलू:
- आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन को सुरक्षा से जोड़ना।
- आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोशिशें।
- मानवाधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना।
- भारत वैश्विक स्तर पर निरस्त्रीकरण, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में योगदान के लिए प्रतिबद्ध है।
निष्कर्ष
समकालीन विश्व में सुरक्षा की अवधारणा अब केवल सैन्य बल तक सीमित नहीं है। यह अब एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलू शामिल हैं। वैश्विक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वार्ता और बहुपक्षवाद ही सबसे प्रभावी रास्ते हैं।