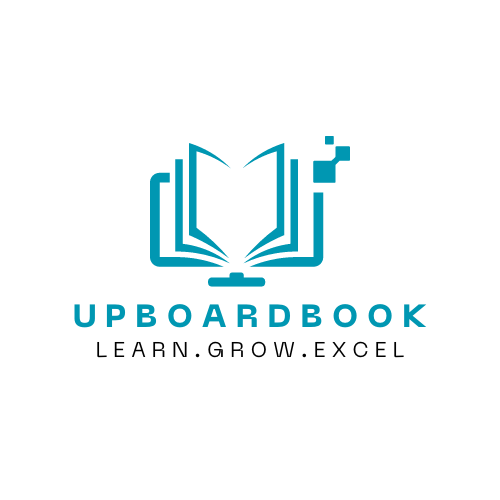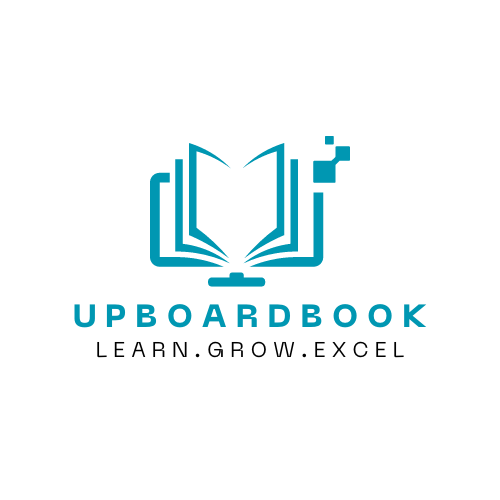UP Board class 12 Geography Chapter 6. द्वितीयक क्रियाऐ Hindi Medium Notes - PDF
अध्याय 6: द्वितीयक क्रियाएँ
यह अध्याय विनिर्माण उद्योगों, जिन्हें द्वितीयक क्रियाएँ भी कहा जाता है, के बारे में है। इनमें कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, जिससे उनका मूल्य बढ़ जाता है।
द्वितीयक क्रियाओं की विशेषताएँ
- ये क्रियाएँ कच्चे माल को निर्मित माल में बदलती हैं।
- इनमें विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण शामिल हैं।
- ये उद्योग मूल्यवर्धन (Value Addition) करते हैं।
- ये रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं।
उद्योगों का वर्गीकरण
उद्योगों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है:
1. कच्चे माल के आधार पर
- कृषि आधारित उद्योग: कपास, जूट, चीनी, वनस्पति तेल आदि।
- खनिज आधारित उद्योग: लोहा-इस्पात, सीमेंट, एल्युमीनियम आदि।
- रासायनिक आधारित उद्योग: उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स, दवाइयाँ आदि।
2. उत्पादों के आधार पर
- आधारभूत उद्योग: ये ऐसे उद्योग हैं जिनके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में काम आते हैं, जैसे लोहा-इस्पात, मशीन टूल्स।
- उपभोक्ता उद्योग: ये ऐसे उद्योग हैं जो सीधे उपभोक्ताओं के लिए तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे कपड़ा, चीनी, कागज, इलेक्ट्रॉनिक सामान।
3. पूंजी निवेश के आधार पर
- छोटे पैमाने के उद्योग: कम पूंजी निवेश वाले उद्योग।
- बड़े पैमाने के उद्योग: अधिक पूंजी निवेश वाले उद्योग।
4. स्वामित्व के आधार पर
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग: सरकार के स्वामित्व वाले, जैसे - BHEL, SAIL।
- निजी क्षेत्र के उद्योग: व्यक्तियों या कंपनियों के स्वामित्व वाले।
- संयुक्त क्षेत्र के उद्योग: सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त स्वामित्व वाले।
- सहकारी क्षेत्र के उद्योग: सहकारी समितियों द्वारा संचालित, जैसे - अमूल।
उद्योगों का स्थानीयकरण (Localization of Industries)
किसी उद्योग के किसी विशेष स्थान पर स्थापित होने को उद्योग का स्थानीयकरण कहते हैं। इसके लिए उत्तरदायी कारक:
- कच्चे माल की उपलब्धता: उद्योग अक्सर कच्चे माल के स्रोत के नजदीक लगाए जाते हैं ताकि परिवहन लागत कम हो।
- शक्ति के साधन: कोयला, तेल, बिजली जैसे ऊर्जा स्रोतों की निकटता।
- परिवहन की सुविधा: रेल, सड़क, बंदरगाह आदि की उपलब्धता।
- श्रम की उपलब्धता: सस्ते और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता।
- बाजार: तैयार माल को बेचने के लिए बाजार की निकटता।
- जलवायु: कुछ उद्योगों के लिए विशिष्ट जलवायु की आवश्यकता होती है।
- सरकारी नीतियाँ: सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए दी जाने वाली छूट और सुविधाएँ।
प्रमुख उद्योग
1. लोहा-इस्पात उद्योग
- यह एक आधारभूत उद्योग है।
- इसके लिए भारी मात्रा में कच्चा माल (लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, चूना पत्थर) लगता है।
- इसलिए, इस उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल की उपलब्धता से प्रभावित होता है।
- भारत के प्रमुख इस्पात केंद्र: जमशेदपुर (झारखंड), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), भिलाई (छत्तीसगढ़), बोकारो (झारखंड)।
2. सूती वस्त्र उद्योग
- यह एक प्राचीन और प्रमुख उपभोक्ता उद्योग है।
- पहले यह उद्योग कच्चे माल (कपास) के क्षेत्रों के आस-पास केंद्रित था।
- आज इसके स्थानीयकरण में बाजार, श्रम, परिवहन आदि कारकों का भी योगदान है।
- मुंबई, अहमदाबाद, कोयंबटूर, इंदौर प्रमुख केंद्र हैं।
3. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) उद्योग
- यह एक नवीन और तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है।
- इसके स्थानीयकरण के लिए मुख्य कारक हैं: उच्च शिक्षित और कुशल श्रमिक, अच्छी संचार सुविधाएँ, बिजली की निर्बाध आपूर्ति और जीवन की उच्च गुणवत्ता।
- बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम (गुड़गाँव) प्रमुख IT हब हैं।
उद्योगों से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे
- वायु प्रदूषण: उद्योगों से निकलने वाली विषैली गैसें (जैसे CO2, SO2) और धुआँ वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं।
- जल प्रदूषण: उद्योगों का अपशिष्ट जल नदियों और जल स्रोतों को प्रदूषित करता है।
- भूमि प्रदूषण: ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण से भूमि की गुणवत्ता खराब होती है।
- ध्वनि प्रदूषण: बड़ी मशीनों और यंत्रों से होने वाला शोर।
उद्योगों का प्रतिरूप (Pattern of Industries)
उद्योगों के स्थानिक वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवर्तन हो रहा है।
- पारंपरिक कारकों (जैसे कच्चा माल, ऊर्जा) का महत्व कम हो रहा है।
- नए कारकों जैसे ज्ञान (Knowledge), तकनीक (Technology) और बाजार (Market) का महत्व बढ़ रहा है।
- उद्योग अब ऐसे क्षेत्रों में स्थापित हो रहे हैं जहाँ इन नए संसाधनों की बेहतर पहुँच है, न कि केवल भौतिक संसाधनों के आधार पर।
निष्कर्ष
द्वितीयक क्रियाएँ या विनिर्माण उद्योग किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। ये रोजगार सृजित करते हैं, मूल्यवर्धन करते हैं और आर्थिक विकास को गति देते हैं। हालाँकि, इनके द्वारा होने वाले पर्यावरणीय degradation को रोकने के लिए सतत विकास (Sustainable Development) के सिद्धांतों पर चलना अत्यंत आवश्यक है।