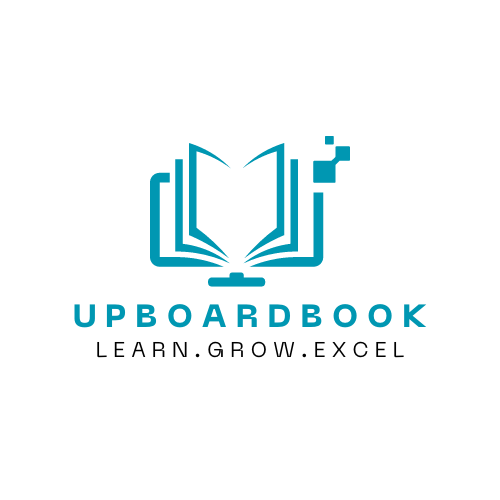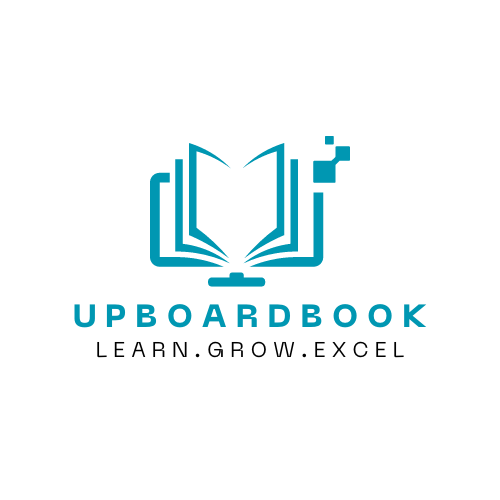UP Board class 11 Geography Chapter 6. मृदा Hindi Medium Notes - PDF
अध्याय 6: मृदा (Soil)
मृदा क्या है?
मृदा या मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो चट्टानों के टूटने और जैविक पदार्थों के मिश्रण से बनती है। यह पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है और पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है।
मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक
- मूल पदार्थ (Parent Material): जिस चट्टान से मृदा का निर्माण होता है, उसकी रासायनिक और भौतिक विशेषताएं मृदा के प्रकार को प्रभावित करती हैं।
- उच्चावच (Topography): ढाल की स्थिति मृदा की गहराई और जल निकासी को प्रभावित करती है।
- जलवायु (Climate): तापमान और वर्षा चट्टानों के अपक्षय और मृदा निर्माण की गति को निर्धारित करते हैं।
- जैविक कारक (Biological Factors): पौधों, जीव-जंतुओं और सूक्ष्मजीवों की क्रियाएं मृदा में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाती हैं और उसकी उर्वरता को प्रभावित करती हैं।
- समय (Time): मृदा के परिपक्व होने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है।
मृदा की विशेषताएँ
- बनावट (Texture): मृदा में मौजूद रेत, गाद और मृत्तिका (चिकनी मिट्टी) के अनुपात को दर्शाती है।
- संरचना (Structure): मृदा कणों के आपस में जुड़ने के तरीके को कहते हैं, जैसे- दानेदार, ग्रन्थित, आदि।
- रंग (Colour): मृदा का रंग उसमें मौजूद कार्बनिक पदार्थ और खनिजों के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए, लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति और काला रंग कार्बनिक पदार्थ की अधिकता को दर्शाता है।
- porosity और पारगम्यता (Porosity and Permeability): मृदा में हवा और पानी रखने और उसे गुजरने देने की क्षमता।
भारत में मृदा के प्रकार
1. जलोढ़ मृदा (Alluvial Soil)
- विस्तार: उत्तरी मैदान और नदी घाटियाँ (सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र), पूर्वी तटीय मैदान।
- विशेषताएँ: नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। रेत, गाद और मृत्तिका का मिश्रण। पोटाश, फॉस्फोरिक अम्ल और चूना से भरपूर, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की कमी।
- फसलें: गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास आदि की खेती के लिए उपजाऊ।
2. काली मृदा (Black Soil / Regur Soil)
- विस्तार: दक्कन के पठार का अधिकांश भाग (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु)।
- विशेषताएँ: काले रंग की, चिकनी और गहरी मिट्टी। लौह, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिना से भरपूर। नमी धारण करने की अच्छी क्षमता। सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं।
- फसलें: कपास की खेती के लिए आदर्श, इसलिए इसे 'कपास की मिट्टी' भी कहते हैं। साथ ही अरहर, गन्ना, ज्वार आदि।
3. लाल और पीली मृदा (Red and Yellow Soil)
- विस्तार: प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र (ओडिशा, छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश)।
- विशेषताएँ: लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण। पीला रंग जलयोजन के कारण होता है। रेतीली और कम उपजाऊ।
- फसलें: बाजरा, दालें, मूंगफली आदि।
4. लैटेराइट मृदा (Laterite Soil)
- विस्तार: उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र (पश्चिमी घाट, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्य)।
- विशेषताएँ: तीव्र निक्षालन के कारण बनती है। लोहे और एल्युमिनियम के ऑक्साइड से भरपूर, लेकिन नाइट्रोजन, पोटाश, चूना कम। इमारत बनाने की ईंटों के लिए उपयुक्त।
- फसलें: चाय, कॉफी, काजू, रबर की खेती के लिए उर्वरक डालकर उपयोग की जाती है।
5. शुष्क/मरुस्थलीय मृदा (Arid/Desert Soil)
- विस्तार: राजस्थान, गुजरात के शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र।
- विशेषताएँ: रेतीली, भुरभुरी, हल्के भूरे रंग की। जैविक पदार्थ की कमी। नमक की मात्रा अधिक।
- फसलें: सिंचाई करके बाजरा, ज्वार, ग्वार आदि उगाई जाती हैं।
6. वन/पर्वतीय मृदा (Forest/Mountain Soil)
- विस्तार: पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र (हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट)।
- विशेषताएँ: पर्वतों पर वनस्पति के सड़ने-गलने से बनती है। अम्लीय प्रकृति की, कम उपजाऊ। ढालू地形 के कारण परतें पतली होती हैं।
- फसलें: चाय, फल, मसाले, बागवानी फसलें।
मृदा अपरदन (Soil Erosion)
मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत का हवा, पानी या अन्य कारकों द्वारा बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है।
- कारण: वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, ढालू भूमि पर खेती, अनुचित कृषि पद्धतियाँ।
- प्रकार: चादर अपरदन, गully अपरदन, वायु अपरदन।
- रोकथाम के उपाय: वृक्षारोपण, समोच्च जुताई, सीढ़ीनुमा खेत बनाना, shelterbelts लगाना, रक्षक मेखला (Shelter Belts) बनाना।
मृदा संरक्षण (Soil Conservation)
मृदा की गुणवत्ता और उर्वरता को बनाए रखने और उसे नष्ट होने से बचाने के उपायों को मृदा संरक्षण कहते हैं।
- बंधियाँ (Contour Bunding) और सीढ़ीदार खेती (Terrace Farming)।
- फसल चक्र (Crop Rotation) अपनाना।
- रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कम्पोस्ट और हरी खाद का प्रयोग।
- वाटरशेड प्रबंधन (Watershed Management)।