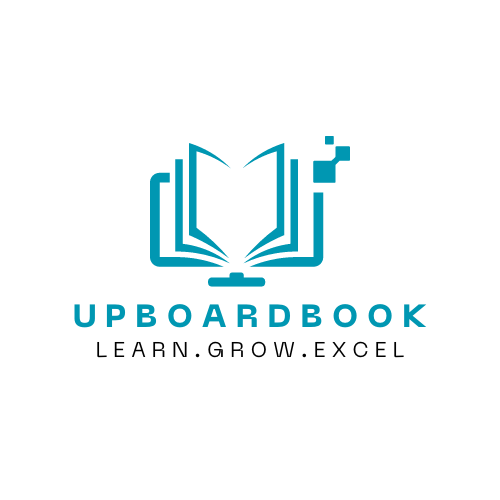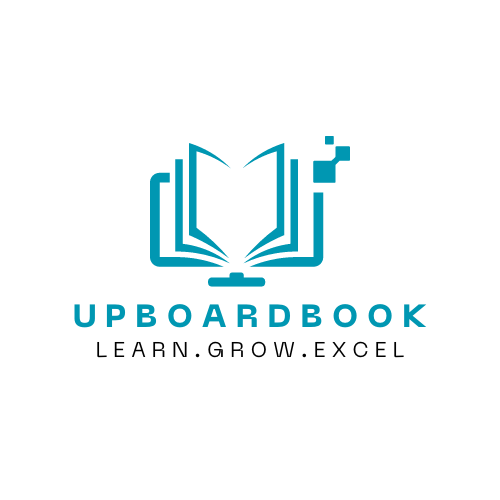UP Board class 11 Geography Chapter 7. प्राकृतिक संकट तथा आपदाएँ Hindi Medium Notes - PDF
अध्याय 7: प्राकृतिक संकट तथा आपदाएँ
यह अध्याय प्राकृतिक खतरों और आपदाओं के बीच के अंतर, उनके प्रकार, कारणों और प्रबंधन के बारे में बताता है।
प्राकृतिक खतरा (Natural Hazard) क्या है?
- प्राकृतिक खतरा एक प्राकृतिक प्रक्रिया या घटना है जो मानव जीवन, संपत्ति और गतिविधियों के लिए खतरा (थ्रेट) पैदा करती है।
- जब तक यह घटना मानव समुदाय को प्रभावित नहीं करती, इसे सिर्फ एक प्राकृतिक घटना माना जाता है।
- उदाहरण: एक सुनामी का खुले समुद्र में उठना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन जब वही सुनामी तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ती है तो वह एक खतरा बन जाती है।
प्राकृतिक आपदा (Natural Disaster) क्या है?
- जब एक प्राकृतिक खतरा मानव समुदाय पर विनाशकारी प्रभाव डालता है, तो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं।
- इसके परिणामस्वरूप जान-माल का भारी नुकसान होता है और स्थानीय संसाधन इतने नष्ट हो जाते हैं कि बाहरी सहायता के बिना सामान्य स्थिति में लौटना मुश्किल हो जाता है।
- उदाहरण: 2004 की सुनामी, 2001 का गुजरात भूकंप, 1999 का उड़ीसा चक्रवात।
प्राकृतिक खतरों के प्रकार
प्राकृतिक खतरों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:
1. जलवायविक खतरे (Atmospheric Hazards)
- ये खतरे वायुमंडल में होने वाली प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं।
- उदाहरण:
- तूफान (चक्रवात, टॉरनेडो)
- बाढ़
- सूखा
- ओलावृष्टि
- तड़ित झंझा (थंडरस्टॉर्म) और आंधी
- हिमस्खलन और हिमतूफान
- लू (Heat Wave) और शीत लहर (Cold Wave)
2. भौगोलिक खतरे (Geological Hazards)
- ये खतरे पृथ्वी की आंतरिक या बाह्य प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं।
- उदाहरण:
- भूकंप
- सुनामी
- ज्वालामुखी विस्फोट
- भूस्खलन और मृदा अपरदन
आपदा प्रबंधन (Disaster Management)
आपदा प्रबंधन आपदा के पहले, दौरान और बाद में की जाने वाली कार्रवाइयों की एक श्रृंखला है। इसे मुख्य रूप से तीन चरणों में बाँटा जाता है:
1. पूर्व-आपदा प्रबंधन (Pre-Disaster Management)
- रोकथाम (Prevention): आपदा आने की संभावना को कम करने के उपाय (जैसे- बाढ़ नियंत्रण के लिए बाँध बनाना)।
- शमन (Mitigation): आपदा के प्रभाव को कम करने के उपाय (जैसे- भूकंपरोधी मकान बनाना, मैंग्रोव वन लगाकर चक्रवात के प्रभाव को कम करना)।
- तैयारी (Preparedness): आपदा से निपटने के लिए पहले से योजना बनाना। इसमें शामिल है:
- पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) विकसित करना
- अभ्यास (मॉक ड्रिल) करवाना
- राहत सामग्री का पहले से भंडारण करना
- जनता में जागरूकता फैलाना
2. आपदा के दौरान प्रबंधन (Management during Disaster)
- इस चरण का मुख्य उद्देश्य जीवन की रक्षा करना है।
- खोज और बचाव अभियान (Search and Rescue Operations) चलाना।
- तत्काल राहत कार्य प्रदान करना जैसे- भोजन, पानी, दवाई और अस्थायी आश्रय।
3. आपदा के बाद का प्रबंधन (Post-Disaster Management)
- पुनर्वास (Rehabilitation): प्रभावित लोगों को उनके सामान्य जीवन में वापस लाने के उपाय (जैसे- मकान बनाना, रोजगार देना)।
- पुनर्निर्माण (Reconstruction): क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे (Infrastructure) जैसे सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल आदि को फिर से बनाना।
- मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना।
भारत में आपदा प्रबंधन
- भारत में आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
- NDMA आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाएँ और दिशा-निर्देश बनाता है।
- राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) कार्य करते हैं।
- राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) विशेष रूप से प्रशिक्षित बल है जो आपदा के समय खोज और बचाव कार्य करता है।
नागरिकों की भूमिका
- आपदा प्रबंधन सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, आम नागरिकों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है।
- स्वयं सहायता (Self-help) और पड़ोसियों की मदद (Community help) आपदा के समय सबसे पहले और सबसे प्रभावी सहायता होती है।
- आपदाओं के बारे में जागरूक होना और तैयार रहना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।